कैसे भारत में वायरल महामारियों की जमीन तैयार कर रहा जलवायु परिवर्तन
कोरोना बाद भारत सहित पूरी दुनिया भविष्य की महामारी पर जोर दे रही है ताकि समय रहते बचाव किया जा सके जबकि भारत में वायरल महामारियों की निगरानी रिपोर्ट एक नई चुनौती की तस्वीर बयां कर रही है जिसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन केवल मौसम की चुनौती नहीं, बल्कि संभावित महामारी का संकेतक बन चुका है।
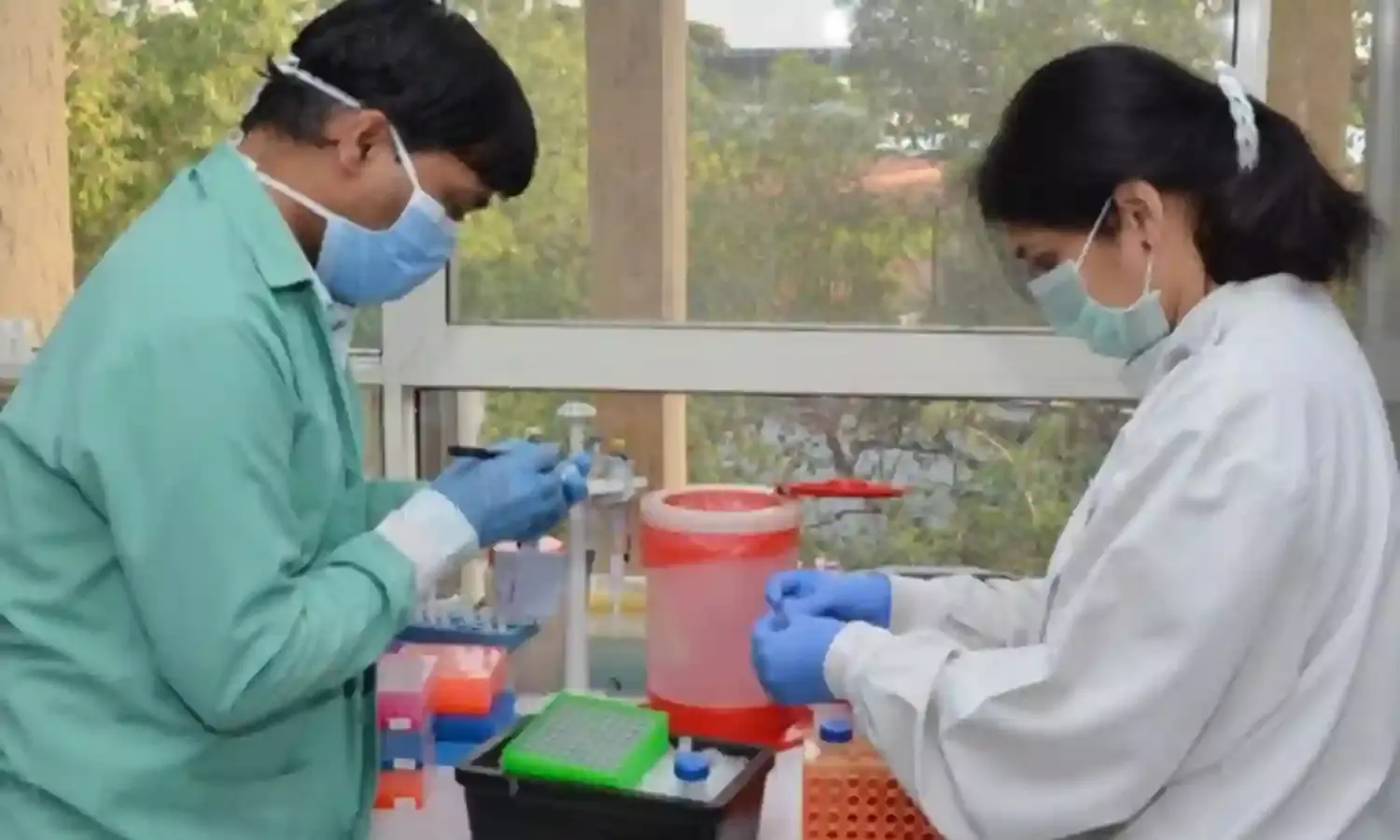
एनआईवी लैब में सैंपल की जांच करते वैज्ञानिक, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
नई दिल्ली: केरल में निपाह, गुजरात में चांदीपुरा, कर्नाटक में मंकी फीवर, गोवा में जीका, दिल्ली में इन्फ्लूएंजा और उत्तर प्रदेश में जापानी एन्सेफलाइटिस। भारत में लगभग हर राज्य के साथ एक संक्रामक बीमारी का नाम बीते कुछ दशक में जुड़ गया है। हालांकि अब यह नाम एक से दूसरे राज्य की यात्रा भी करने लगा है यानी धीरे धीरे बीमारी अन्य क्षेत्रों को भी अपने दायरे में ले रही है।
यह जानकारी आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के वैज्ञानिकों ने दी है जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रयोगशालाओं में लगातार नई और पुरानी वायरल बीमारियों की निगरानी रख रहे हैं। इनके मुताबिक, भारत अब उन देशों में शामिल है जहां क्लाइमेट-लिंक्ड वायरल इमर्जेंस की घटनाएं सबसे तेजी से बढ़ रही हैं।
एनआईवी ने साझा एक प्रेजेंटेशन में जानकारी दी है कि बीते दो दशक में कई नए वायरस भारत में सामने आए हैं। नए उभरे वायरस में निपाह (2001), क्राइमियन-कांगो हेमरेजिक फीवर (2011), वेस्ट नाइल (2011), जीका (2016), कोविड-19 (2020), मंकीपॉक्स (2022) और एच5एन1/एच5एन2 इन्फ्लुएंजा (2024–25) जबकि दोबारा उभरे वायरस में हमारे सामने चांदीपुरा और क्यासानूर वन रोग (केएफडी) जिसे आम भाषा में मंकी फीवर भी कहते हैं। इनके अलावा लंबे समय से आबादी के लिए जोखिम बने डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और हेपेटाइटिस ए और ई प्रसारित हैं।आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने विदर्भ में प्रसारित सिकलसेल के जीवित वायरस को कुछ इस तरह दिखाया, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
दरअसल जलवायु परिवर्तन का मतलब तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव से है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता में यह बदलाव रोगजनकों और उनके वेक्टरों के व्यवहार में परिवर्तन की वजह भी बन रहा है जिससे इनके संचरण के नए मार्ग खुलने की आशंका होने लगी है। यही कारण है कि भारतीय वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन और वायरल महामारियों को आपस में जोड़ते हुए नए सिरे से निगरानी प्रणाली पर काम कर रहे हैं।
दो दशक में कई नए वायरस
इंडियास्पेंड से बातचीत में नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की चर्चित वायरोलॉजिस्ट डॉ. प्रज्ञा यादव ने कहा, "हम अभी तक जलवायु परिवर्तन का मतलब धरती के बढ़ते ताप, भीषण गर्मी या फिर अत्यधिक बारिश जैसे उदाहरणों से जोड़कर देख रहे हैं जबकि हम यह नहीं जानते कि यह बदलाव भारत में वायरल महामारियों के लिए एक नई जमीन भी तैयार कर रहा है जो भविष्य के लिए गंभीर चुनौती भी बन सकती है।"
नागपुर में बन रहे भारत के एकमात्र और निर्माणाधीन राष्ट्रीय वन हेल्थ इंस्टिट्यूट की जिम्मेदारी संभाल रहीं और कोरोना की पहली स्वदेशी जांच और टीका विकसित करने वालों में से एक डॉ. प्रज्ञा यादव पुणे स्थित आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) की वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं।
उन्होंने बातचीत में यह भी कहा कि धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही इंसान-वन्यजीव संपर्क, अनियमित बारिश और प्राकृतिक आवास में बदलाव ने वायरसों को उभरने का नया रास्ता दे दिया है।
डॉ. प्रज्ञा यादव ने कहा कि गंभीर वायरस के वाहकों मच्छरों और चमगादड़ों के फैलाव को बढ़ावा देने में जलवायु परिवर्तन अहम भूमिका निभा रहा है क्योंकि अनियमित बारिश और बाढ़ से जहां मच्छरजनित और पानी से फैलने वाले संक्रमण बढ़ रहे हैं। वहीं वन्यजीवों के आवास-प्रवास में बदलाव वायरसों को नए क्षेत्रों तक ले जाने में मददगार है। इसी तरह इंसान-वन्यजीव संपर्क कृषि विस्तार और शहरीकरण वायरसों के स्पिलओवर को आसान बना रहा है।
जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण बना मंकी फीवर
डॉ. प्रज्ञा यादव ने कहा कि भारत में जलवायु परिवर्तन से वायरल महामारियां जो नई जमीन तैयार कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण मंकी फीवर यानी क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज (केएफडी) है। भारत के पश्चिमी घाट से फैलता यह टिक-बोर्न खतरा वर्षों तक कर्नाटक में सीमित रहा। साल 1957 में पहली बार इसकी चपेट में आने वाला मरीज कर्नाटक में मिला लेकिन अब (2015-2024) यह कर्नाटक से गोवा, महाराष्ट्र और केरल तक प्रसारित हुआ है। इसके एंडेमिक ज़ोन लगातार बड़े हो रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि भारत को टिक-बोर्न बीमारियों की निगरानी और वैक्सीन रणनीति को तत्काल मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए।
केएफडी से आम आदमी के बचाव को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा, "पिछले कुछ समय से वैज्ञानिकों की पूरी टीम इस बीमारी से बचाव के लिए टीका की खोज में जुटी हुई है। एनआईवी की टीम का शोध जारी है जो आईआईएल यानी इंडियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर एक निष्क्रिय सहायक टीका विकसित कर रही है।"टीबी के संदिग्ध सैंपल की प्रयोगशाला में जांच करती वैज्ञानिक, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
ICMR–NIV के निदेशक डॉ. नवीन कुमार से साझा प्रेजेटेंशन में जलवायु परिवर्तन के चलते जीका वायरस की रिपोर्टिंग में आए बदलाव को कुछ इस तरह समझाया गया, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
भारत का निगरानी केंद्र एनआईवी
वायरल बीमारियों को लेकर भारत का सबसे बड़ा केंद्र पुणे स्थित आईसीएमआर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) है जहां बीएसएल 4 स्तर तक की प्रयोगशाला है जिसमें कोरोना को सबसे पहले न सिर्फ आइसोलेट किया गया बल्कि उससे पहला स्वदेशी टीका भी बनाया गया।
भविष्य की महामारियों को लेकर यह भारत का सबसे बड़ा निगरानी केंद्र भी है। भारत के प्रत्येक राज्य को निगरानी में लाने के लिए एनआईवी ने पुणे के अलावा जम्मू, डिब्रूगढ़, जबलपुर और बेंगलुरु चार जोनल प्रयोगशाला और मुंबई, केरल एवं बेंगलुरु में तीन फील्ड यूनिट भी स्थापित की हैं।
एनआईवी निदेशक डॉ. नवीन कुमार ने मानव इतिहास में कई विनाशकारी महामारियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में लगभग सभी तरह के वायरस को वर्गीकरण करने की जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय समिति पर है जिसे आईसीटीवी कहा जाता है। यह समिति भारत में 1971 से वायरस इतिहास पर काम कर रही है।
54 साल में 50 गुना वायरस भारत के कब्जे में
साल 1971 तक 290 विषाणु प्रजातियां, 43 वंश और उनके दो परिवार के बारे में भारतीय वैज्ञानिकों के पास जानकारी थी। समय के साथ यह जानकारी बढ़ती गई और साल 2002 तक हमारे पास 1602 विषाणु प्रजातियां, 247 वंश और 70 परिवार की जानकारी एकत्रित हुई। लंबे प्रयास और संसाधनों का विकास होने के बाद 2023 में भारत के पास 14690 विषाणु प्रजातियां, 3522 वंश और उनके 314 परिवारों के बारे में जानकारी मिली है।
जलवायु परिवर्तन और भारत में नई वायरल महामारियों के बारे में जानकारी देते एनआईवी के निदेशक डॉ. नवीन कुमार, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि लगभग हर दिन नए वायरस या फिर उनके आनुवंशिक प्रकारों की सूचना मिल रही है। बढ़ता वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई नए रोगजनकों के उद्भव में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कुछ वायरसों के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन अधिकांश वायरल संक्रमणों के लिए हमारे पास प्रभावी एंटीवायरल दवाओं का अभाव है।
हर राज्य में मिल रहा एक अलग प्रकोप
भौगोलिक दृष्टिकोण से कैसे भारत में वायरल महामारियों की तस्वीर बन रही है। इसके मुताबिक, केरल में साल 2018 से 2023 के बीच चमगादड़ों से निपाह संक्रमण का प्रसार हुआ है जबकि साल 2024 में गुजरात में चांदीपुरा का प्रकोप बीते 20 वर्षों में सबसे बड़ा देखा गया। इसी तरह गोवा और बिहार में साल 2023 के दौरान जीका वायरस में ट्रांसमिशन यानी आबादी में तेजी से फैलने वाले नए म्यूटेशन दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, गोवा में क्यासानूर वन रोग (केएफडी) की नई लहर सामने आई है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा में जापानी एन्सेफलाइटिस ने अपनी जमीन तैयार की है जो एक विषाणु जनित रोग है और गंभीर जटिलताओं से लेकर मृत्यु तक का कारण बनती है।
इंसानों के अलावा पशुओं में संक्रामक रोग भी निगरानी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए एनआईवी ने पशु विषाणुओं को लेकर जानकारी दी है कि साल 2019 में गांठदार त्वचा रोग यानी लंपी वायरस और अफ़्रीकी स्वाइन फीवर कई राज्यों में दर्ज किया गया जो पहले बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता था।
डॉ. नवीन कुमार बताते हैं कि भारत में जो वायरल संक्रमण जन स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा बने हुए हैं उनमें डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, जीका वायरस के अलावा इन्फ्लूएंजा वायरस, हेपेटाइटिस बी, सी और जापानी एन्सेफलाइटिस हैं। साथ ही इनसे अपेक्षाकृत उपेक्षित वायरस में आंतों के वायरल संक्रमण और हेपेटाइटिस ए व ई सक्रिय हैं।
बच्चों को रोटा वायरस संक्रमण से बचाने के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिस पर आईसीएमआर के शोध की जानकारी दी गई, स्त्रोत परीक्षित निर्भय
भारत में 73 जगहों पर बना सिंड्रोमिक सर्विलांस नेटवर्क
एक सवाल पर इंडिया स्पेंड से बातचीत में डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि रेस्पिरेटरी वायरस पर निगरानी रखने के लिए हाल ही में भारत ने सिंड्रोमिक सर्विलांस नेटवर्क सक्रिय किया है जो अलग अलग राज्यों में 73 साइटों से रियल-टाइम डाटा दे रहा है। इससे नए वेरिएंट और मौसमी रुझानों की पहचान में करने में मदद मिल रही है। इसमें शहरों से लेकर गांव और सीमावर्ती स्थान तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अलग-अलग जलवायु और जनसंख्या प्रोफाइल में वायरस प्रसार का पैटर्न समझना है।
यह पूछे जाने कि कितने तरह के वायरस की निगरानी की जा रही है, इस पर डॉ. नवीन कुमार ने बताया कि चार प्रमुख रोगजनकों का बहुस्तरीय परीक्षण किया है जिसमें इन्फ्लूएंजा, कोविड-19, आरएसवी और निपाह वायरस (पश्चिम बंगाल और केरल) शामिल है। इस नेटवर्क के जरिए अर्ली वार्निंग अलर्ट पर काम किया जा रहा है। यानी नए वेरिएंट या संक्रमण में अचानक वृद्धि पर राज्यों को चेतावनी जारी करना और पॉलिसी इनपुट यानी टीकाकरण रणनीति, अस्पताल तैयारी और जनस्वास्थ्य दिशा-निर्देश तय करने में मदद करना।
आईसीएमआर के मुताबिक, इस सिंड्रोमिक सर्विलांस नेटवर्क की बदौलत अब तक कई तरह के आउटब्रेक का समय पर पता चला है जिसमें जुलाई 2021 में हरियाणा से H5N1, मार्च 2024 (H9N2) पश्चिम बंगाल से, अप्रैल 2025 (आंध्र प्रदेश से) और मई 2025 में उडुपी कर्नाटक से दूसरा H5N1 मामला पता चला। इन वायरस को आइसोलेट करने के बाद आगे का शोध भी जारी है।


